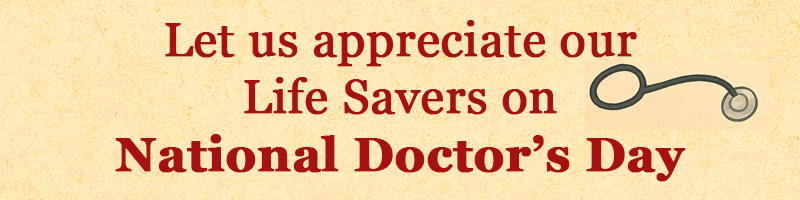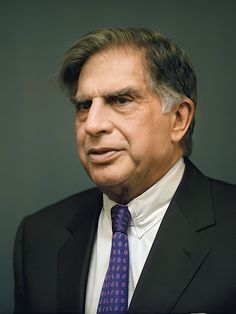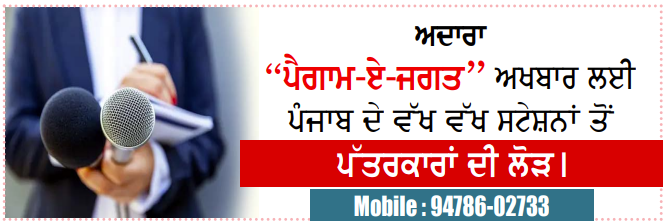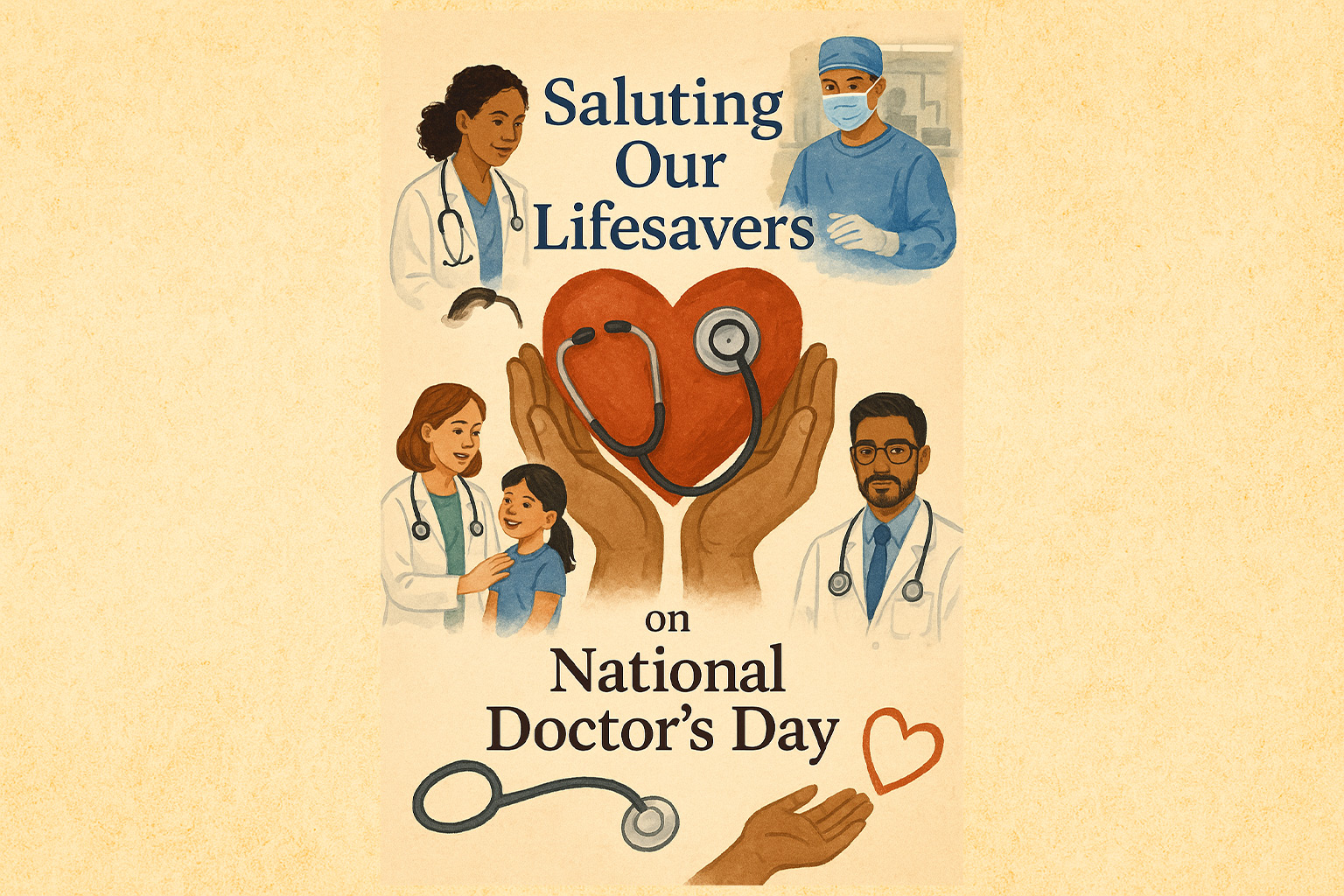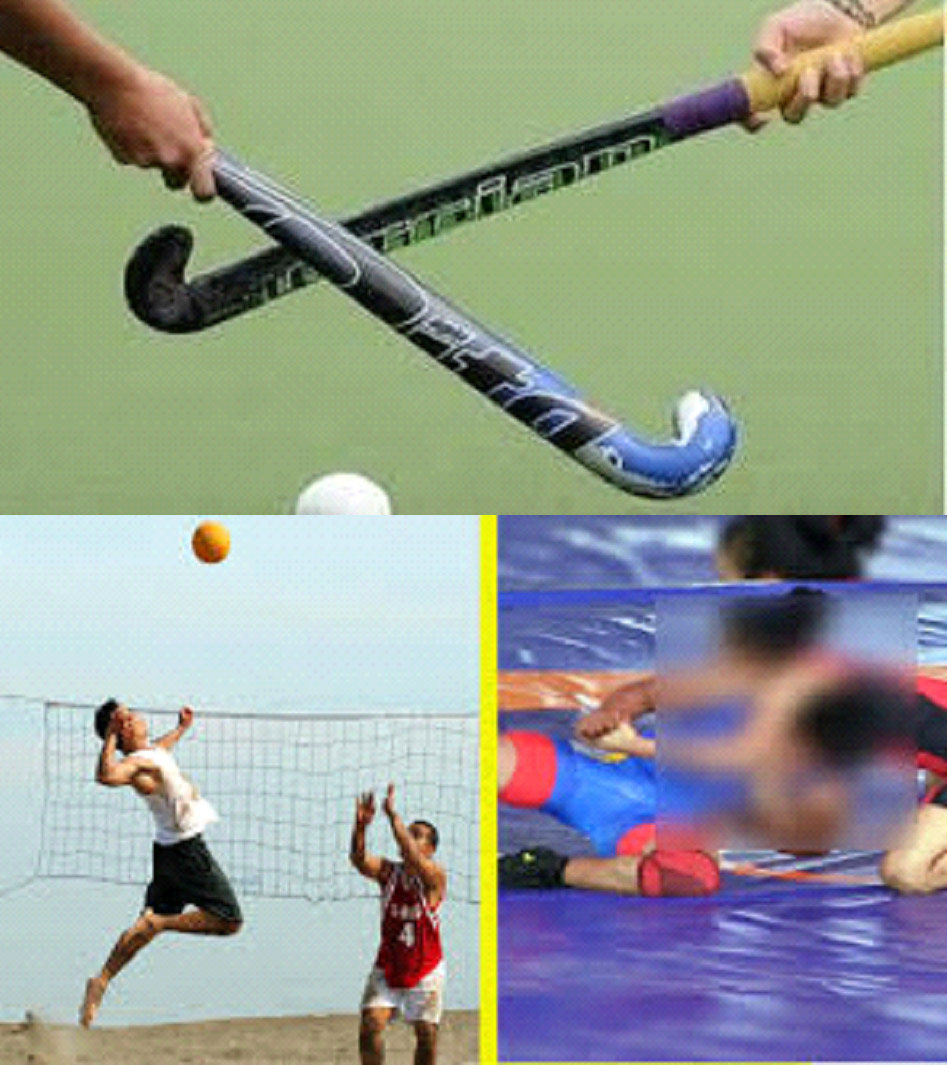हमारे नौजवानों के दर्द को सुनने की ज़रूरत
पिछले कुछ हफ़्तों में चंडीगढ़ और आस-पास के इलाकों में कई युवाओं ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन यह संवेदनशील ख़बर भी शायद ज़्यादातर लोगों के लिए अनसुनी ही रह गई। सत्रह — यह सिर्फ़ एक आंकड़ा नहीं है। ये उजड़े हुए परिवार, कभी न पूरे होने वाले सपने और अधूरी रह गई कहानियाँ हैं। इन घटनाओं की ख़ामोशी हमें एक गंभीर सच्चाई बता रही है: हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ नौजवान अंदर से टूट रहे हैं, लेकिन उनकी पुकार बार-बार अनसुनी रह जाती है।
पिछले कुछ हफ़्तों में चंडीगढ़ और आस-पास के इलाकों में कई युवाओं ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन यह संवेदनशील ख़बर भी शायद ज़्यादातर लोगों के लिए अनसुनी ही रह गई। सत्रह — यह सिर्फ़ एक आंकड़ा नहीं है। ये उजड़े हुए परिवार, कभी न पूरे होने वाले सपने और अधूरी रह गई कहानियाँ हैं। इन घटनाओं की ख़ामोशी हमें एक गंभीर सच्चाई बता रही है: हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ नौजवान अंदर से टूट रहे हैं, लेकिन उनकी पुकार बार-बार अनसुनी रह जाती है।
आज का नौजवान एक अदृश्य युद्ध में फँसा हुआ है — कामयाब होने के दबाव और असफलता के डर के बीच। सोशल मीडिया पर चमकदार जीवन दिखाने की होड़ ने उनकी असली भावनाओं को दबा दिया है। इस तेज़ रफ्तार दुनिया में हर ओर आगे बढ़ने की दौड़ है, लेकिन भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं। उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए भावनात्मक साथ नहीं मिल रहा। बचपन से ही नंबर, प्रदर्शन, परीक्षा, अच्छी नौकरी और माता-पिता की उम्मीदों को पूरा करना — यह सब बिना रुके चलता रहता है। यह दबाव इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति कभी खुद को पूरा महसूस नहीं कर पाता।
इन युवाओं को अपना दर्द साझा करना नहीं सिखाया जाता। हम उनकी भावनाओं को हल्के में ले लेते हैं: “यह तो उम्र का असर है,” या “सब ठीक हो जाएगा।” लेकिन यह बातें उस व्यक्ति के लिए जानलेवा बन सकती हैं जो मुश्किल समय से गुज़र रहा हो। बच्चों को असफलता, हार और निराशा से निपटना नहीं सिखाया जाता — उन्हें सिर्फ़ अधूरापन मिलता है। नरमी को कमज़ोरी मान लिया गया है। थेरेपी को अभी भी बहुत से लोग “आख़िरी उपाय” मानते हैं, न कि एक स्वस्थ रास्ता।
कुछ उम्मीद जगाने वाले क़दम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने डिजिटल माध्यमों से सहायता शुरू की है। हेल्पलाइन नंबरों पर मदद उपलब्ध है। कुछ राज्यों ने स्कूलों में काउंसलिंग के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, और कुछ जगहों पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर पाठ्यक्रम लागू हो रहे हैं। लेकिन ये सेवाएँ अभी भी काफी सीमित हैं। गाँवों और छोटे क़स्बों में इनकी पहुँच लगभग न के बराबर है।
सरकार को यह मानना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। हर स्कूल और कॉलेज में लाइसेंसशुदा और अनुभवी काउंसलर होने चाहिए। हर ज़िले में ऐसे सलाह केंद्र हों जो आम लोगों के लिए सुलभ और सस्ते हों। मानसिक स्वास्थ्य पर चलने वाले अभियान केवल एक दिन या एक बार नहीं, बल्कि पूरे साल, विभिन्न भाषाओं और मीडिया माध्यमों से होने चाहिए। थेरेपी को इंश्योरेंस कवरेज में शामिल किया जाना चाहिए।
लेकिन सिर्फ़ नीतियाँ ही काफ़ी नहीं हैं। हमारी सोच भी बदलनी चाहिए। माता-पिता को अपने बच्चों से दिल से बात करनी चाहिए, बिना फ़ैसला सुनाए उन्हें सुनना चाहिए। अध्यापकों को यह समझना होगा कि छात्र की ख़ामोशी अक्सर सबसे ऊँची चीख होती है। दोस्तों को सिर्फ़ “कैसे हो?” पूछने की बजाय गंभीरता से समझना होगा कि शब्दों के पीछे क्या छुपा है। कई बार सिर्फ़ किसी के साथ रहना, बिना उपदेश दिए, सबसे बड़ी मदद हो सकती है।
अगर आप अंदर से टूट रहे हैं, तो समझिए — आप अकेले नहीं हैं। आपका दर्द जायज़ है। आपको यह बोझ अकेले नहीं ढोना। रोना, डरना, कमज़ोर लगना — यह सब सामान्य है। मदद माँगिए। किसी दोस्त, माता-पिता या काउंसलर के पास जाइए। अगर एक दरवाज़ा बंद है, तो दूसरे को खटखटाइए। कोशिश जारी रखिए। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ख़ामोशी से संघर्ष कर रहा है, तो उसके पास जाइए। पूछिए, दर्द बाँटिए और सुनिए।
ये ज़िंदगियाँ सिर्फ़ एक आंकड़ा बन कर न रह जाएँ। यह हमारे लिए चेतावनी की घड़ी बने। आइए, हम ऐसी दुनिया बनाएँ जहाँ मदद माँगना सामान्य हो, न कि शर्म की बात। इलाज शुरू होता है — बात करने, सुनने और ईमानदारी से स्वीकारने से। हम ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहाँ कोई भी अपने दर्द में अनसुना न रहे और कोई भी अकेला न महसूस करे।
— दविंदर कुमार