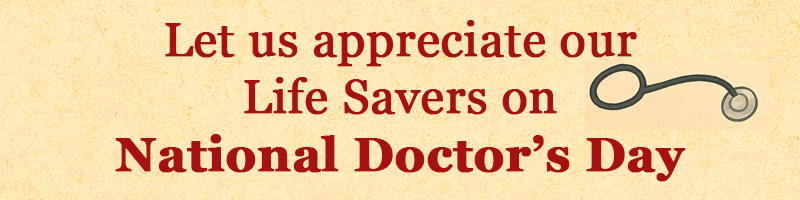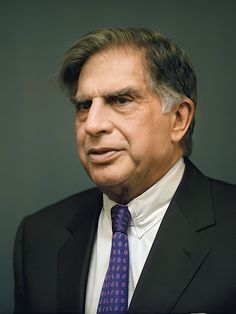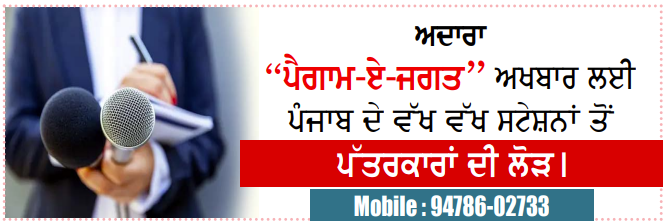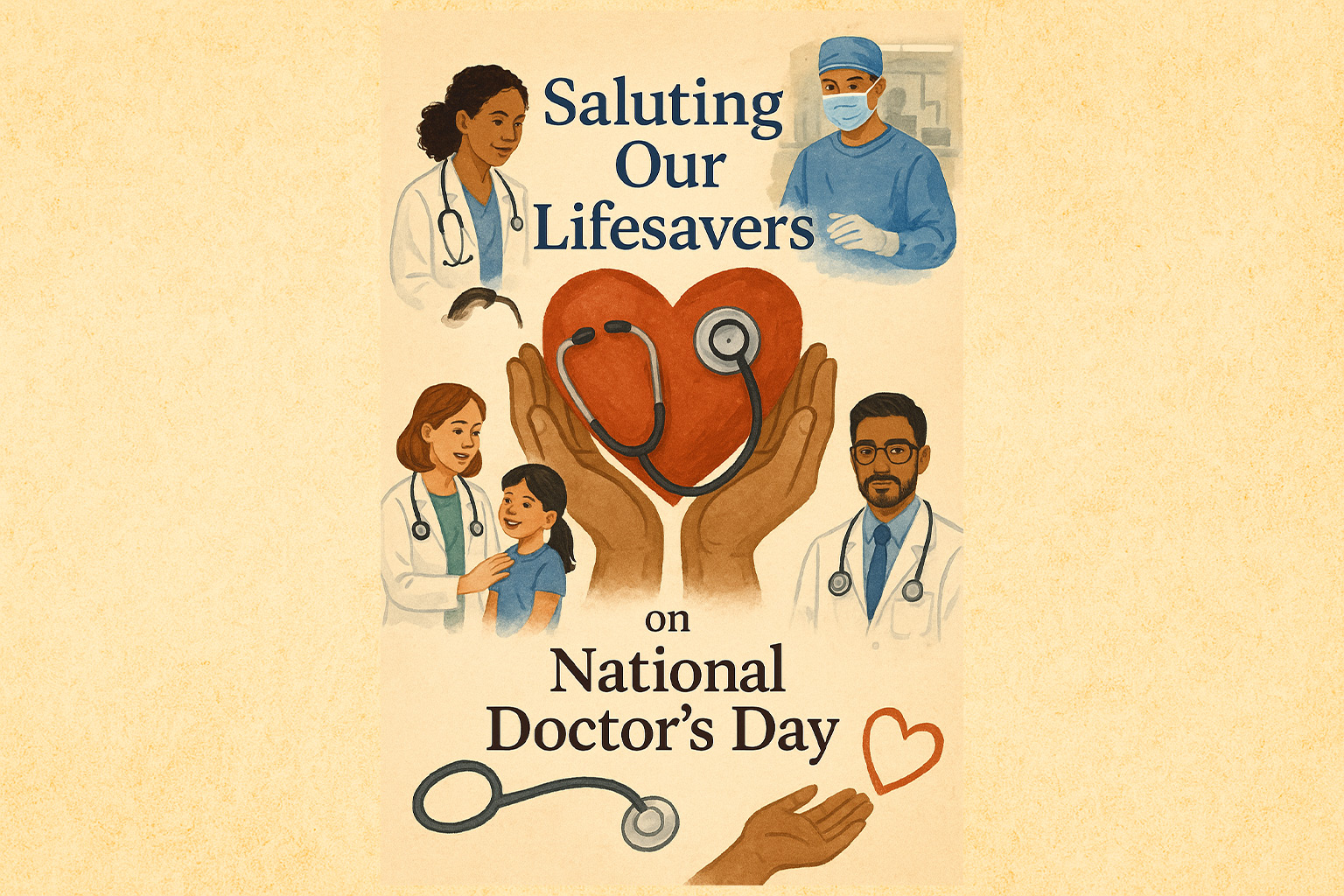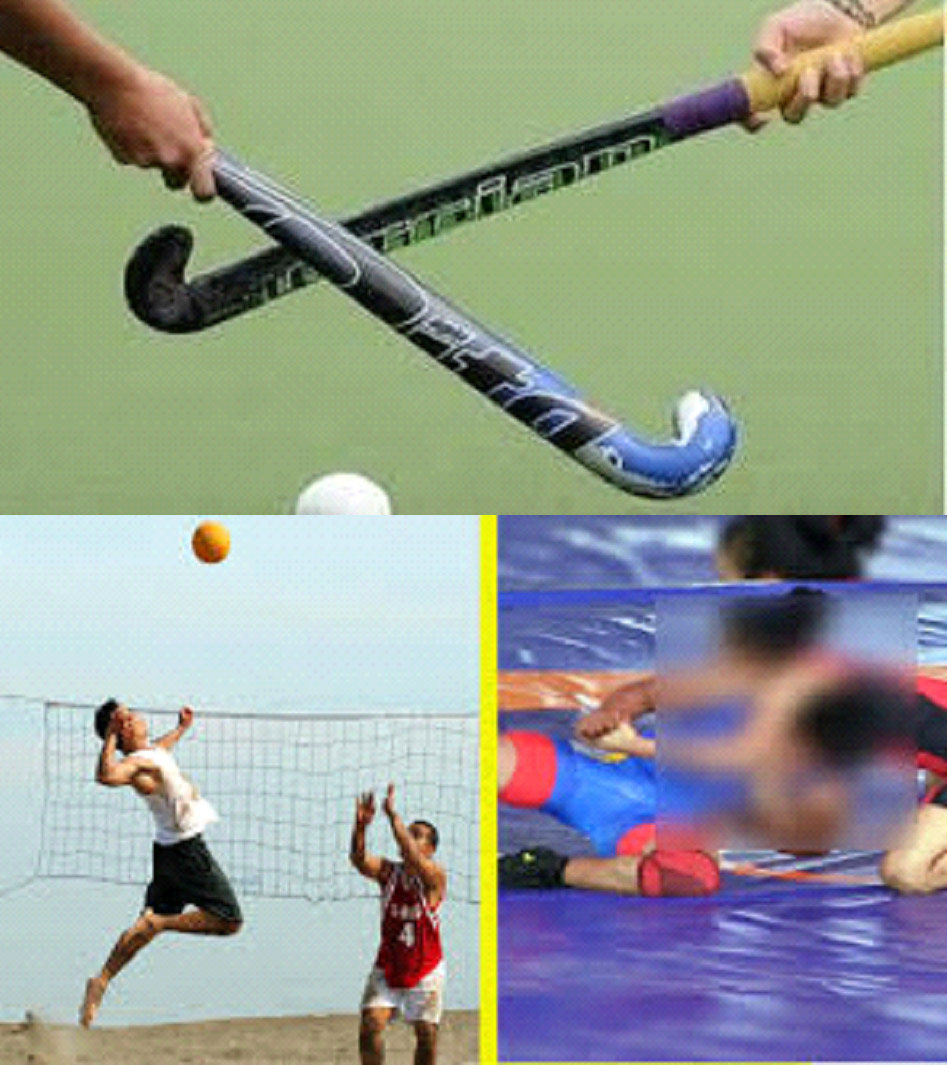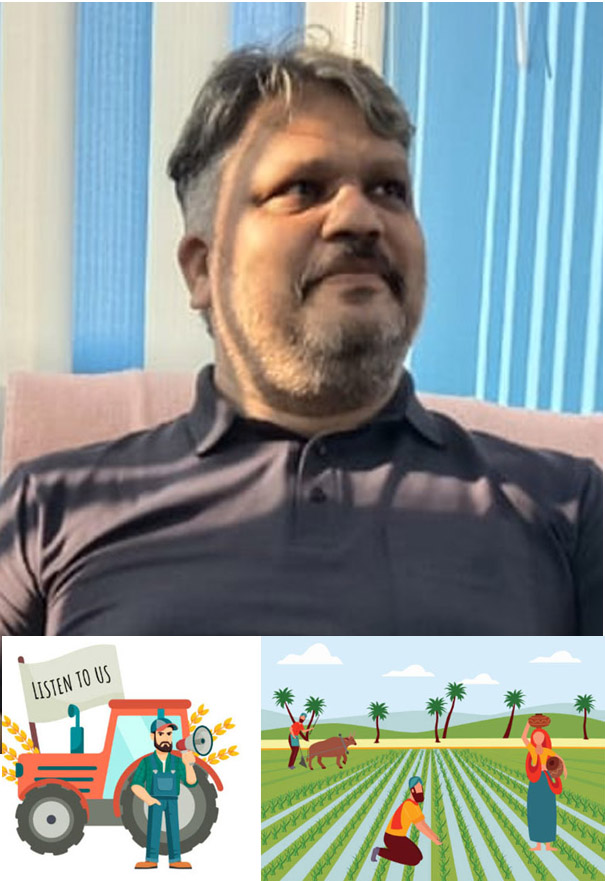
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध के अधिकार का संरक्षण
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण और पोषित अधिकारों में से एक है, जो दुनिया भर के संविधानों में निहित है। भारत में, यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित है, जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के अधिकार की गारंटी देता है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण और पोषित अधिकारों में से एक है, जो दुनिया भर के संविधानों में निहित है। भारत में, यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित है, जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के अधिकार की गारंटी देता है।
जब नागरिकों की बात नहीं सुनी जाती है, तो वे अभिव्यक्ति और विरोध के माध्यम से अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं। ये अधिकार लोकतंत्र में दबाव के रूप में कार्य करते हैं, जिससे उन्हें असहमति व्यक्त करने और शिकायतों को दूर करने की क्षमता मिलती है।
विरोध निराधार नहीं हैं। वे अनसुनी शिकायतों, प्रणालीगत त्रुटियों या गलत नीतियों का परिणाम हैं। किसानों के लिए, विरोध अक्सर उनके जीवन, परंपराओं और अस्तित्व के लिए जोखिम भरा होता है। ये लोग अपने खेतों और घरों को आसानी से नहीं छोड़ते। विरोध में एक साथ आना हताशा की अभिव्यक्ति है।
जब किसान विरोध करते हैं, तो यह केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं होता है, बल्कि जीवन और मृत्यु का मामला होता है। उनकी मांगें, जो उनके जीवन की कठोर वास्तविकताओं से जुड़ी होती हैं, अक्सर तर्क की मदद से प्रस्तुत की जाती हैं।
लोकतंत्र में हर संवाद का आधार सुनना है। यह एक नैतिक दायित्व है। सुनना यह पहचानना है कि हर नागरिक की आवाज़ मायने रखती है। किसान, जो हमारे भोजन के प्रदाता हैं, हमारे समाज में एक अलग और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 18% का योगदान करते हैं और 40% से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। किसानों के विरोध के कारण को समझने के लिए, हमें सतही तौर पर सोचना होगा।
वे 23 प्रमुख फसलों के लिए गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं ताकि बाजार में उतार-चढ़ाव से स्वतंत्र, उचित और सुसंगत मूल्य सुनिश्चित हो सके। उनका तर्क है कि एक स्थिर, अनुमानित एमएसपी उनकी आजीविका की रक्षा करेगा और उन्हें उत्पादन लागतों को पूरा करने की अनुमति देगा। मौजूदा प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए एक सूत्र-आधारित दृष्टिकोण की मांग कर रहे हैं, जो उत्पादन की वास्तविक लागत, मुद्रास्फीति और बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखता है।
यह वार्षिक विवेकाधीन-आधारित पद्धति की जगह लेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि एमएसपी फसलों के वास्तविक मूल्य को दर्शाता है। क्षेत्रों के बीच एमएसपी दरों में असमानता इस मुद्दे को और जटिल बनाती है। पंजाब और हरियाणा के किसानों को गेहूँ और चावल के लिए उच्च एमएसपी दरें मिलती हैं, लेकिन ये कीमतें अभी भी उत्पादन लागत से कम हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से तनावग्रस्त हैं। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी वित्तीय परेशानियाँ बढ़ गई हैं। पंजाब में, अत्यधिक चावल की खेती ने भूजल संसाधनों को कम कर दिया है, जिससे यह प्रथा अस्थिर हो गई है।
किसान विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और पर्यावरणीय दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की वकालत कर रहे हैं। किसान एक एकीकृत, राष्ट्रव्यापी एमएसपी प्रणाली की भी मांग कर रहे हैं जो सभी क्षेत्रों में समान मूल्य सुनिश्चित करे, असमानताओं को दूर करे और स्थान की परवाह किए बिना फसलों के लिए उचित मुआवजा प्रदान करे। इसके अलावा, वे सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के साथ फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने का आग्रह करते हैं, क्योंकि इस तरह के समर्थन के बिना, किसान चावल जैसी पानी की अधिक खपत वाली फसलों की खेती जारी रखने के लिए मजबूर महसूस करते हैं, जो केवल पर्यावरणीय मुद्दों को बदतर बनाता है।
आलोचकों ने अक्सर कहा है कि विपक्ष समानता को बाधित करता है और असुविधा पैदा करता है। हालांकि यह कुछ हद तक सच हो सकता है, लेकिन बड़ी कठिनाई यह है कि इन विरोधों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को अनदेखा किया जाए। लोकतंत्र असहमति और विचारों के गतिशील आदान-प्रदान पर पनपता है। विरोध को दबाना, चाहे बलपूर्वक हो या हताशा से, इस संतुलन को नष्ट कर देता है। जब समाज का एक हिस्सा- खासकर किसानों जैसे महत्वपूर्ण हिस्से की बात नहीं सुनी जाती, तो यह संगठन के लिए खतरा बन जाता है और लोकतंत्र से समझौता करता है। एक लोकतंत्र जो अपने असंतुष्टों की बात नहीं सुनता, वह खतरे में है।
अर्थहीन संवाद का मतलब है कि जनता और सरकार के बीच एक खाई पैदा होती है, जो अलगाव और अविश्वास को जन्म देती है। यह अलगाव सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक भी है। हर विरोध के पीछे एक मानवीय कहानी होती है। किसानों के लिए, यह उनकी पिछली पीढ़ियों के संयुक्त प्रयासों, भूमि के लिए भावुक श्रम और उनके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के सपने की कहानी है। जब इन कहानियों को नजरअंदाज किया जाता है, तो यह उन लोगों को असमान महसूस कराता है जो हमारी आजीविका हैं। किसानों की आर्थिक कठिनाइयाँ इस तथ्य से और भी बढ़ जाती हैं कि वे अदृश्य हैं। विरोध करना आशा का कार्य है- एक विश्वास कि उनकी आवाज़ सुनी जा रही है और उनकी समस्याओं को पहचाना जा रहा है। जब यह आशा निराशा या प्रतिरोध से मिलती है, तो इससे न केवल सरकार पर उनका भरोसा खत्म हो जाता है, बल्कि न्याय के प्रति उनकी बुनियादी उम्मीद भी खत्म हो जाती है।
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि विरोध करने का अधिकार सार्वभौमिक है। विरोध करने का अधिकार हर मांग पर सहमत होने के बारे में नहीं है, बल्कि इस सिद्धांत को स्वीकार करने के बारे में है कि हर आवाज सुनी जानी चाहिए।
विरोध को नज़रअंदाज़ करने का मतलब है उन लोगों की मानवता को नज़रअंदाज़ करना। कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी पीड़ा, उनके भय और उनकी आशाओं का कोई मूल्य नहीं है। यह सही नहीं है और यह लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों के खिलाफ है।
किसानों के विरोध प्रदर्शन का समाधान, और सभी विरोध प्रदर्शनों का समाधान, वास्तविक बातचीत में निहित है। खुले मन से सुनना और करुणा से जुड़ना सिर्फ सरकारी कार्य नहीं है, यह एक मानवीय कार्य है। आम सहमति से तैयार किए गए समाधान अधिक स्थायी होते हैं।
अंततः, किसी भी समाज का मापदंड यह है कि वह अपने सबसे कमजोर वर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। देश को भोजन देने वाले किसान न केवल हमारे आभार के पात्र हैं, बल्कि हमारे ध्यान और सम्मान के भी पात्र हैं। उनका विरोध लोकतंत्र के मूल्यों की पुष्टि है, उसके खिलाफ नहीं।