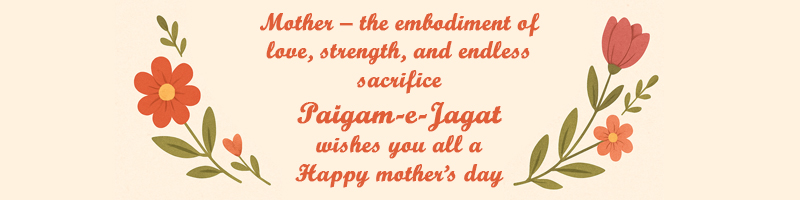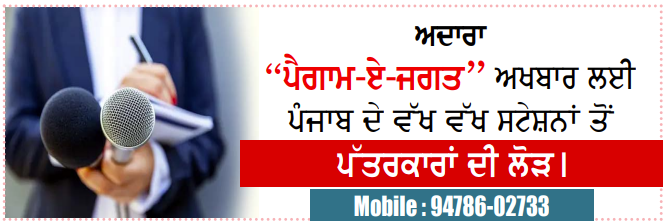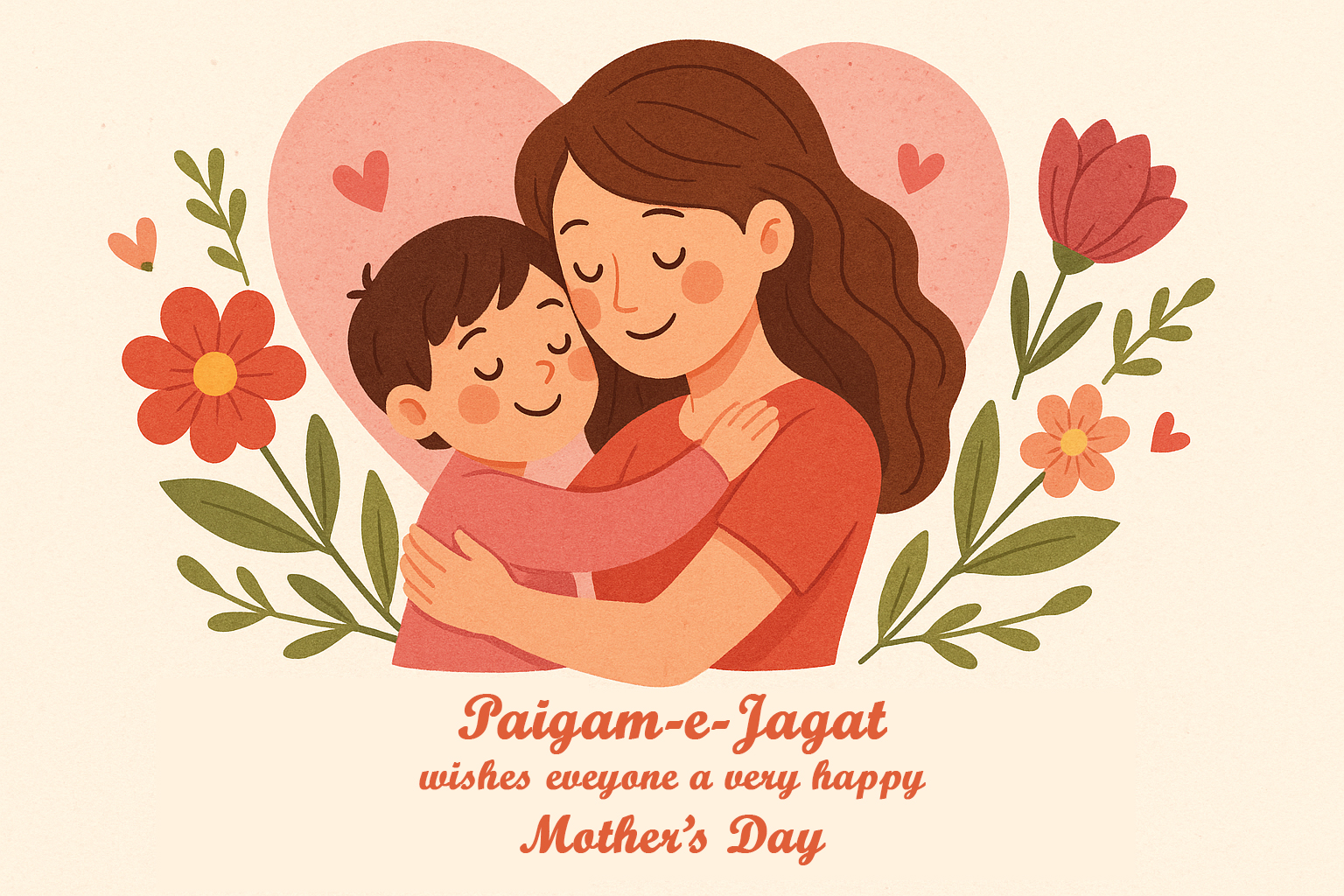लाल फीताशाही: आम नागरिक के धैर्य की परीक्षा
मालवा के प्रसिद्ध पंजाबी कवि जगसीर जीदा, जो अपनी कविताओं के लिए मंचीय कवि के रूप में विख्यात हैं, की एक पंक्ति है:
मालवा के प्रसिद्ध पंजाबी कवि जगसीर जीदा, जो अपनी कविताओं के लिए मंचीय कवि के रूप में विख्यात हैं, की एक पंक्ति है:
"धीयां शगुन स्कीमां नू उड़िकन,
कुछड़ नियाणे चुक के "
यह पंक्ति हमारी नौकरशाही की कार्यकुशलता और लाल फीताशाही पर गहरा व्यंग्य है। वास्तव में, यह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई को दर्शाती है। हमारी अर्ज़ियाँ, मांग पत्र, और जायज़ हक की सूचियाँ फाइलों की धीमी गति में अटक जाती हैं। शायद यह प्रथा केवल भारत में ही है। बहरहाल, हम अपने देश और उसकी चिंताओं की ही बात करना पसंद करेंगे। "लाल फीताशाही" शब्द एक फाइल को लाल रंग की डोरी से बाँधने की परंपरा से उत्पन्न हुआ है। पुराने समय से ही लोगों की अर्ज़ियाँ, शिकायतें, और मांग पत्रों को गत्ते पर रखकर, उसे चारों ओर से मोड़े गए रंगीन कागज़ से ढककर, रंगीन रस्सी या डोरी से बाँध दिया जाता था। आज भी, कागज़ों का एक पुलिंदा फाइल फोल्डर में रखकर, उसे रंगीन तस्मे जैसी डोरी से बाँधकर संबंधित कर्मचारी, अधिकारी, या मंत्री के डेस्क पर रख दिया जाता है। इसके बाद, वह फाइल एक डेस्क से दूसरी डेस्क या अलग-अलग हाथों से होकर अपने अंतिम पड़ाव तक पहुँचती है, जहाँ अंतिम फैसला लिया जाता है। लेकिन इसमें कितना समय लगेगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि लाल फीताशाही का मतलब है फैसला लेने और निपटारे में देरी। यह देश के लोगों के लिए एक त्रासदी है और देश के लिए अभिशाप सिद्ध होती है।
यदि इस समस्या के कारणों की बात करें, तो पहला प्रमुख कारण है कई अनावश्यक और जटिल नियम, जिन्हें समझना और पालन करना आम आदमी के लिए असंभव हो जाता है। कई बार ये नियम अधिकारियों की समझ से भी परे होते हैं, जिसके कारण फैसला लेने में देरी होती है। अक्सर अधिकारी जानबूझकर टालमटोल करते हैं या फैसला लेने से कतराते हैं। इसका सीधा नुकसान संबंधित व्यक्ति या समूह को होता है। इससे उनमें निराशा और बेचैनी पैदा होती है। इसके परिणामस्वरूप, आम लोगों का सरकारी तंत्र से विश्वास उठ जाता है, और कल्याणकारी नीतियों को लागू करने में बड़ी बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।
समय के बदलाव के साथ लोगों में काफी जागरूकता आई है। सरकारों और प्रशासनिक तंत्र ने समय के मूल्य को समझते हुए कुछ सुधार किए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है सूचना का अधिकार। 2005 में लागू इस कानून का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार को रोकना, और लोकतंत्र को सही मायनों में जनकल्याणकारी बनाना था। इसके लागू होने से काफी हद तक हालात सुधरे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए प्रयास करती रहती हैं। डिजिटल तकनीकों, जैसे कि इन्वेस्ट इंडिया और पेपरलेस ग्रीन क्लीयरेंस, के ज़रिए कागज़ी कार्यवाही को कम किया जा रहा है और सरकारी सेवाओं को तेज़ किया जा रहा है। सरकारी तंत्र में कुशलता लाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे नई तकनीकों को अपनाने और लागू करने में सक्षम हो सकें।
हालांकि दशकों पुरानी आदतों और परंपराओं को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रयास ज़रूरी हैं। इसलिए, प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है कि वे निर्धारित समय में फैसला लें। नौकरशाही में नेतृत्व, जनसेवा, ईमानदारी, और सही फैसले लेने की क्षमता को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। आम लोगों को शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता के खिलाफ सहायता प्रदान करने के लिए लोकपाल व्यवस्था को मज़बूत करके प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। आज के समय में कार्यों के निपटारे में अनावश्यक देरी और लाल फीताशाही एक बड़ी नैतिक गिरावट है, जिससे जनसाधारण का सरकारी कार्यप्रणाली में विश्वास कम होता है। प्रभावी शासन के लिए लाल फीताशाही को लाल कालीन में बदलने की आवश्यकता है।
-दविंदर कुमार
- देविंदर कुमार